पवनों के प्रकार
पिछले अध्याय में हमने समझाकि एक गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, पवन के कितने प्रकार हैं? वैज्ञानिकों ने इनमे पाए जाने वाले विशेष गुणों के आधार पर इनको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है.
सनातनी पवनें (permanent wind ) जो सनातन काल से बहती है
सावधि पवनें एक निश्चित अवधि में बहती हैं
प्रवर्तनीय पवनें जो निरंतर परिवर्तित होती हैं
स्थानीय पवनें जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर उत्पन्न होती हैं
सनातनी पवन या स्थायी पवन
व्यापारिक पवनें
उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी (उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध २३ डिग्री से ३५ डिग्री अक्षांश ) से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी (शुन्य अक्षांस ) की और चलती हैं, इन्हे अनावर्ती पवन भी कहते हैं. ३० डिग्री उत्तरी अक्षांश से ३० डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र अनवर्ती क्षेत्र कहलाता है. इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर भी होती यही है इसलिए इन्हे व्यापारिक पूर्वा पवनें भी कहते हैं.
प्राचीन काल में जब मोटर व्हीकल नहीं थे तब समुद्री बेड़े (नाव) पर कपडे बांधकर नाव का संतुलन पवन की दिशा के साथ बनाया जाता था, उस समय यह पवने विभिन्न महाद्वीपों के बीच होने वाले अंतरार्ष्ट्रीय व्यापार में बहुत सहायक होती थीं, इन पवनों के सहारे व्यापारी बहुत आसानी से अपने सामान का परिवहन कर लेते थे. पुराने ज़माने में इनके सहारे अंतररष्ट्रीय व्यापार होता था इसलिए इन्हे व्यापारिक पवन कहा जाता है.
इन पवनों का भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी के क्षेत्र में अभिषरण (मिलन ) होता है उस क्षेत्र को ITCZ ZONE (INTER TROPICAL CONVERSION ZONE (अन्तः अनवर्ती अभिषरण क्षेत्र ) कहा जाता है, जैसा की विदित हो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत मौसम पाया जाता है, अगर उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, यह पवने विपरीत सवभाव के तापमान वाली होती हैं एक गर्म एक ठंडी, जब विपरीत स्वभाव की पवन आपस में टकराती है तो संघनन होता है वर्षा होती है, इसकी कारन यह क्षेत्र सर्वाधिक् वर्षा वाला क्षेत्र है क्योंकि यहाँ लम्बे समय तक अन्तः अन्वर्ती पवनो का अभिषरण होता रहता है. (जिसका मुख्य कारण सूर्य की निरंतर किरणे यहां पर पड़ना है और निम्न वायु दाब को बढ़ाना है )
पछुआ पवन
उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से (अश्व अक्षांश ) उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलती हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह,सदैव इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की और होती है. जिस कारण इन्हे पछुआ पवनें कहते हैं यह पवनें भी निरंतर चलती है.
यह पवन ३० डिग्री से ६५ डिग्री अक्षांश उत्तरी एवं दक्षिणी गोलरार्द्ध दोनों जगह चलती है हमें संसार का नक्शा देखने की जरूरत है अगर आप अवलोकन करें तो पाएंगे, जहां उत्तरी गोलार्ध में कई महाद्वीप स्थित हैं या भू स्थल अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री या जल क्षेत्र अधिक है. इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में इन पछुआ पवनों की त्रीवता निरंतर बढ़ती जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में बिना किसी पर्वत ग्लेसियर (भू क्षेत्र ) से टकराये इनका त्रीव वेग बना रहता है.
दक्षिणी गोलार्ध में चलते हुए जब यह समुद्र की लहरों को चीरकर चलती हैं तब बहुत शोर मचता है इसी शोर के आधार पर इनको नाम दिया गया है जब यह ४० डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आस पास चलती है तब इन्हे गरजता चालीसा कहा जाता है, जब यह ५० डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आस पास चलती हैं तब इन्हे दहाड़ती पचासा कहा जाता है जब यह ६० डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आस पास चलती हैं तब इन्हे चीखता साठा कहा जाता है.
ध्रुवीय पवनें (पुर्वा पवनें)
८० डिग्री से ९० डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के बीच में चलने वाली पवनों को धुर्वीय पुर्वा पवनें कहा जाता है यह पवन भी वर्ष भर चलती है, इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की और होती है इसलिए इन्हे ध्रुवीय पूर्वा पवनें भी कहते हैं.
इन तीन प्रकार की सनातनी पवनों में दो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है पहली व्यापारिक पवन दूसरी धुर्वीय पूर्वा पवन और एक पश्चिम से पूर्व की और चलती है जिसे पछुआ पवन कहा जाता है. जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है या वायुदाबीय पेटियों का निर्माण हुआ है तब से यह पवन निरन्तर चलती रहती है इसलिए इन्हे सनातनी या स्थायी पवन कहा जाता है.
सावधि पवनें
इन पवनो का निर्माण एक निश्चित अवधि या समय के लिए होता है इसलिए इन्हे सावधि पवन कहते है जिनके मुख्य उदहारण हैं मानसूनी पवनें और स्थलीय समीर और समुद्रीय समीर
मानसूनी पवन
जैसे की विदित हो पृथ्वी के सूर्य के चारो ओर चक्कर लगाने के कारन सूर्य ६ महीने कर्क रेखा पर लंबवत होता है मतलब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और ६ महीने मकर रेखा पर लंबवत होता है मतलब दक्षिणी गोलारार्ध में गर्मी का मौसम होता है ठीक इसके विपरीत दोनों गोलार्धो में सर्दी का मौसम होता है.
अगर दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होगा तो वहाँ की ठंडी पवन उत्तरी गोलार्ध की ओर चलेगी क्योंकि वहां गर्मी के कारन निम्न वायुदाब का निर्माण हो चुका है (जैसा की पहले भी कहा गया है पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती है) ठीक इसी तरह अगर उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होगा तो यहाँ की ठंडी पवन निम्न दाब क्षेत्र अर्थार्त दक्षिण गोलार्ध की और चलेगी।
चूँकि इन पवनो का निर्माण एक निश्चित अवधि केलिए होता है इसलिए इन्हे सावधि पवन कहते हैं
स्थलीय समीर और समुद्रीय समीर
दिन में स्थल सूर्य की गर्मी से अधिक गर्म हो जाते हैं इसलिए समुद्र की ठंडी पवन स्थल की और चल पड़ती है ठीक इसी प्रकार रात में स्थल ठन्डे रहते है और समुद्र गर्म तो पवन स्थल से समुद्र की ओर चल पड़ती है.
मछुआरे रात में मछली पकड़ते हैं क्योंकि पवन की दिशा समुद्र की ओर होती है जो उनकी नाव को बिना इसी अधिक प्रयास के समुद्र में अधिक दूर तक ले जाती है, और वह दिन में वापस आते हैं क्योंकि अब पवन की दिशा स्थल की ओर है और उनकी नव आसानी से तट की और आ जाती है.
घाटी समीर और पर्वतीय समीर
यह पवन पहाड़ी क्षेत्रो में चलती हैं दिन के समय घाटी गर्म हो जाती पवन अपने समीपस्थ पर्वत के सहारे ऊपर उठ जाती है और उस पर्वत की ऊंचाई पर स्थित ठंडी पवन से टकरा जाती है जिससे संघनन के कारण बादल बन जाते है (जिनका घर या होटल किसी घाटी के नजदीक वाले पर्वत पर हो वह इन् बादलो का नजारा कर सकते है. यह घटना घाटी समीर के कारण होती है जो केवल दिन में ही चलती है ठीक इसके विपरीत रात में पर्वत से घाटी की ओर पवन चलती है जिसे पर्वतीय समीर कहा जाता है, यह रत में ही चलती है.
चूँकि इन पवनो का निर्माण एक निश्चित अवधि केलिए होता है इसलिए इन्हे सावधि पवन कहते हैं
परिवर्तनीय पवनें
जिन पवनों का कोई निश्चित दिशा या समय नहीं होता और जो कभी भी अपनी दिशा बदल लेती है उन्हें परिवर्तनीय पवन कहते है इनका मुख्य उदाहरण चक्रवात और प्रति चक्रवात है.
हम अक्सर समाचारो में इनके बारे में सुनते है की एक चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ वह चेन्नई के तट पर बढ़ रहा है तभी सुनते हैं की वह विशाखापत्तनम पर बढ़ रहा है बाद में पता चलता है वह म्यांमार या बांग्लादेश में घुस गया है, इस प्रकार इनका कोई निश्चित स्थान या दिशा नहीं, यह अपना गंत्वय बदलते रहते है इसलिए इन्हे परिवर्तनीय पवन कहा जाता है.
स्थानीय पवन
जो पवन एक निश्चित स्थान और निश्चित अवधि के दौरान उत्पन्न होती है उन्हें स्थानीय पवन कहा जाता है, यह लगभग सभी महा द्वीपो पर एक निश्चित अवधि के लिए पाई जाती हैं इनका उदारण, कुछ इस प्रकार है
लू एक गर्म हवा है, भारत में जून जुलाई के दौरान चलने वाली एक गर्म हवा है जो उत्तरी भारत में थार मरुष्ठल से आती है उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली तक पायी जाती है
‘
चिनूक राकी पर्वत से आने वाली एक गर्म हवा है जो USA, CANADA के पशुपालको और चरागाहों के लिए एक वरदान साबित होती है, अमेरिका में इसके नाम के चिनूक हेलीकाप्टर भी बनते हैं
फान आल्पस पर्वत से आने वाली एक गर्म हवा है जो स्विटज़रलैंड के पशुपालको और चरागाहों के लिए बहुत उपयोगी होती है, यह वहां का मौसम खुशनुमा कर देती है.
हरमट्टन सहारा क्षेत्र (अफ्रीका) से चलने वाली एक गर्म हवा है जो गिनी तट पर एक डाक्टर पवन के नाम से जनि जाती है यह वहां की सर्द हवा को गर्म कर देती है इससे वहां के निवासियों के सवास्थ्य में लाभ होता है इसलिए इसे डॉक्टर पवन भी कहते है
सिमुक अरब रेगिस्तान, नार्वेस्टर नूज़ीलैण्ड, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, फायं बैग इंडोनिसिया, ब्लैक रोलर (धूलभरी आंधी ) USA इत्यादि कुछ अन्य स्थानीय पवनो के उदाहरण हैं.
इस प्रकार भूगोल की दृष्टि से हमने हमारी पृथ्वी पर चलने वाली विभिन्न प्रकार की पवनो का परिचय पाने की कोशिश की है, हमें हवा (पवन) की भूगोलिक व्याख्या समझ आए या न आये, इससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता की हवा हमारे आस पास मौजूद रहती है और हम किसी न किसी रूप में उसका अनुभव भी करते है और उनसे प्रभावित भी होते हैं.

KRIPYA PAVAN SE JUDE AUR TATHYO KO JANANE KE LIYE PIECHLE ADHYAY PAR JAYE
******
Share this:
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
- Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Click to share on X (Opens in new window) X
- Click to share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
- Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram

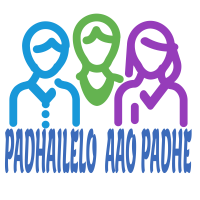




Nice information 🙏🙏🙏
Thanks